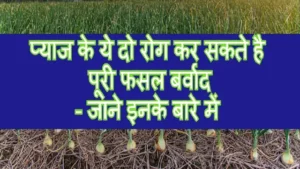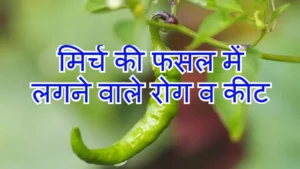Brinjal Insect : बैंगन के पौधों में लगने वाले कीट भारत में बैंगन की खपत आलू के बाद दूसरे नंबर पर आती है. भारत में बैगन के रंग, आकार एवं आकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार की वैरायटी पाई जाती है. किसान भाइयों के लिए यह बहुत ही लाभप्रद खेती है. बैगन की फसल में अनेक प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है. जिसके कारण उत्पादन पर भी गहरा असर पड़ता है. बैंगन की फसल में लगने वाले रोगों के अलावा उनकी रोकथाम पर भी बात करेंगे.
बैंगन के पौधों में लगने वाले कीट
- तना एवं फल बेधक : यह कीट पत्तों के साथ साथ बैंगन को अंदर से भी खा जाते है, जिसके कारण फसल की उपज को नुकसान पहुंचता है.
- लाल मकड़ी : यह लाल मकड़ी पत्तों के नीचे जाल बनाकर पत्तों का रस चूसती है. इसके कारण बैगन के पत्ते लाल रंग के दिखाई देने लगते है.
- जैसिड : इस प्रकार के कीड़े पत्तों के नीचे चिपककर रस चूसते हैं. जिसके कारण पत्तियां का रंग पीला और पौधे कमजोर हो जाते है
- जड़ निमेटोड : इससे पौधों की जड़ों में गांठ बन जाती है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग पीला और पौधों का विकास रूक जाता है. जड़ निमेटोड के ये प्रमुख लक्षण है.
- एपीलैक्ना बीटल : एपीलैक्ना बीटल पत्तों को खाने वाला लाल रंग का छोटा कीड़ा होता है.
बैंगन के पौधों में लगने वाले रोग
सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग (Cercospora Leaf Spot Disease)
रोग – इस रोग से पत्तियों पर कोणिय से लेकर अनियमित महीन धब्बे बनते जाते हैं जोकि बाद में स्लेटी भूरे रंग के हो जाते हैं. इस रोग से प्रभावित पत्तियाँ जल्दी ही गिर जाती हैं.
सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग से रोकथाम (Prevention of Bacterial wilt disease)
रोकथाम – इस रोग की रोकथाम के लिए क्लोरोथलोनिल 75 डबल्यूपी 400 ग्राम या कॉपर ओक्सिक्लोराइड़ 400 ग्राम या फिर मेंकोजेब 75 डबल्यूपी 500 ग्राम प्रति 200 लीटर जल की दर से एक एकड़ में छिड़काव करें..
जीवाणु उखटा रोग (Bacterial Wilt Disease)
यह रोग स्यूडोमोनास सोलेनीसेरम नामक जीवाणु से होता है. फसल पर इस रोग का प्रकोप आने पर पौधों की पत्तियों का मुरझाना, पीलापन तथा पौधा अल्प विकसित होना और बाद में सम्पूर्ण पौधा मुरझा जाता है. इस रोग के कारण पहले पौधे की पत्तियाँ गिरती है और पौधे का संवहन तंत्र भूरा हो जाता है. इस रोग का मुख्य लक्षण शुरुआती अवस्था में पौधा दोपहर के समय मुरझा जाता है और रात में सही हो जाता है लेकिन बाद में समाप्त हो जाता है.
जीवाणु उखटा रोग से रोकथाम (Prevention of Bacterial wilt disease)
- रोग ग्रसित पौधें को खेत से उखाड़ कर जला दें.
- गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें.
- खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था करें
- बीज को कार्बेन्डेजिम 2.5 ग्रा./कि.ग्रा. की दर से उपचारित करें
- फसल चक्र अपनायें।
- रोग प्रतिरोधी प्रजातियां लगाएं.
- क्लोरोथलोनिल 75 डबल्यूपी 2 ग्राम या कसूगामायसिन 5 + कॉपर ओक्सिक्लोराइड़ 45 डबल्यूपी 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करें.
अल्टरर्नेरिया पत्ती धब्बा रोग (Alternaria leaf Spot Disease)
इस रोग के कारण केन्द्र में वलय युक्त धब्बे बनते हैं जो बाद में ये धब्बे बड़े हो जाते हैं. ये धब्बे फलों पर भी दिखायी देने लगते हैं.
अल्टरर्नेरिया पत्ती धब्बा रोग से रोकथाम (Prevention of Alternaria Leaf Spot Disease)
इस रोग से संक्रिमत पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए. इस रोग की रोकथाम के लिए एजोक्सोस्ट्रोबिन 23 एससी 1 मिली या मेटिरम 55%+ पायरोक्लोक्लोस्ट्रोबिन 5 डबल्यूजी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करना चाहिए.
मोजेक और छोटी पत्ती रोग (Mosaic and Little Leaf Disease)
यह एक माइकोप्लाजमा जनित विनाषकारी रोग है. यह रोग ‘लीफ होपर’ नामक कीट से आता है. इस रोग से ग्रसित पौधों का आकर बोना हो जाता है. इस रोग के अन्य लक्षण भी है जैसे पत्तियों पर चितकबरापन व अल्पविकसित होना या पत्तियों का विकृत छोटी एवं मोटी होना आदि है. इस रोग के कारण नई पत्तियाँ सिकुड़ कर छोटी हो जाती है तथा मुड़ भी जाती है तथा पत्तियाँ तने से चिपकी हुई लगती है. जिस कारण से बैगन के पौधों पर फल नहीं बनते हैं अगर फल आ भी जाये तो वो अत्यंत कठोर होते हैं. पौधा झाड़ीनुमा हो जाता हैं.
मोजेक और छोटी पत्ती रोग से रोकथाम (Prevention of Mosaic and Little Leaf Disease)
- यह रोग रसचूसक कीट (Sucking Pest) जैसे लीफ हॉपर (फुदका) और एफीड द्वारा आता है. इस रोग की रोकथाम के लिए एसिटामिप्रीड 20% SP की 80 ग्राम मात्रा या थियामेंथोक्साम 25% WG की 100 ग्राम मात्रा या थियामेंथोक्साम 12.6% + लैम्ब्डा साइहेलोथ्रिन 9.5% ZC मिश्रण की 100 मिली या डायमेथायट 400 मिली मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव प्रति एक एकड़ के हिसाब से करना चाहिए.
- फसल को लीफहोपर से बचने के लिए 0.1 प्रतिषत एकाटोक्स या फोलीडोल का फल निर्माण तक छिड़काव करना चाहिए. पौधों को रोपाई से पूर्व टेट्रासाइक्लिन के 100 पी.पी.एम. घोल में डुबोकर रोपाई करनी चाहिए
- रोग रोधी किस्में जैसे – पूसा पर्पिल क्लस्टर और कटराइन सैल 212 – 1, सैल 252-1-1 और सैल 252-2-1 उगाये. पेड़ी फसल ना लगाएं.
फल सड़न रोग (Fruit Rot Disease)
अधिक नमी के कारण बैगन की फसल में यह रोग अधिक आता है. फंगस की वजह से फलों पर जलीय सूखे हुये धब्बे दिखाई देने लगते है जो बाद में धीरे धीरे दूसरे फलो में भी फैल जाता है. इस रोग से प्रभावित फलों ऊपरी सतह भूरे रंग की हो जाती है जिस पर सफ़ेद रंग के कवक बन जाता है.
फल सड़न रोग से रोकथाम (Management of Fruit Rot Disease)
- इस रोग से फसल को बचने के लिए मेंकोजेब 75% WP की 600 ग्राम मात्रा या कासुगामायसिन 5% + कॉपरआक्सीक्लोराइड 45% WP की 300 ग्राम या हेक्साकोनाज़ोल 5% SC की 300 ग्राम मात्रा या स्ट्रेप्टोमायसिन सल्फेट 90% + टेट्रासायक्लीन हाइड्रोक्लोराइड 10% W/W की 24 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए.
- 15-20 दिनों बाद आवश्यकतानुसार छिड़काव दवा बदल कर करे या जैविक उपचार के रूप में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस की 250 ग्राम या ट्राइकोडर्मा विरिडी की 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर दे.
बैगन का निमेटोड या सूत्रकृमि (Brinjal Nematode)
यह रोग सूत्रकृमि पेलाडोगाइन की अनेक प्रजातियों द्वारा उत्पन्न होता हैं. लगातार नमी के कारण सूत्रकर्मी पैदा हो जाते है. इस रोग से प्रभावित पौधों के जड़ों में गांठों का गुछा बन जाता है. प्रभावित पौधा बोना तथा पत्तियां हरी पीली होकर लटक जाती हैं. इस रोग से पौधा नष्ट तो नहीं होता किन्तु गांठो के सडने पर सूख जाता हैं. नेमाटोड के संक्रमण के कारण अन्य फफूंद भी जड़ों में प्रवेश कर पौधे में रोग फैलाने की अधिक संभावना बढ़ आती है. इस रोग की वजह से फसल में 45-55 प्रतिशत तक हानि होती हैं.
बैगन निमेटोड रोग से रोकथाम (Brinjal Nematode Management Measures)
- गर्मी के मौसम में मिट्टी की गहरी जुताई करे तथा अच्छी तरह से धूप लगने दें.
- जिस खेत में यह रोग है वहाँ 2-3 साल तक बैंगन, मिर्च और टमाटर की फसल न लगाए.
- पौध रोपाई के बाद फसल के चारों ओर या फसल के बीच-बीच में एक या दो पंक्ति में गेंदा को लगाना चाहिए.
- कार्बोफ्यूरान 3 % दानों को पौध रोपाई से पहले 10 किलो प्रति एकड़ की दर से मिला दे.
- निमाटोड के जैविक नियंत्रण के लिए 200 किलो नीम खली या 2 किलो वर्टिसिलियम क्लैमाइडोस्पोरियम या 2 किलो पैसिलोमयीसिस लिलसिनस या 2 किलो ट्राइकोडर्मा हरजिएनम को 100 किलो अच्छी सड़ी गोबर के साथ मिलाकर प्रति एकड़ की दर से जमीन में मिला दे.
- नेभागान 12 लीटर प्रति हैक्टयर की दर से भूमि का फसल बोने या रोपने से 3 सप्ताह पूर्व शोधन करना चाहिए
अगर आपको Brinjal Pests and Control in Hindi से संबन्धित अन्य जानकरी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते है, साथ में यह भी बताएं कि आपको यह लेख कैसा लगा, अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा है आप इस आर्टिकल को शेयर करें.